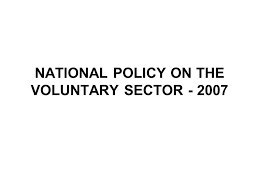
स्वैच्छिक क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति 2007
नीति का दायरा
नीति में, स्वैच्छिक संगठनों (वीओ) का अर्थ नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, परोपकारी या वैज्ञानिक और तकनीकी विचारों के आधार पर सार्वजनिक सेवा में लगे संगठनों को शामिल करना है। स्वैच्छिक संगठनों में औपचारिक और अनौपचारिक समूह शामिल हैं, जैसे:
- समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ)
- गैर-सरकारी विकास संगठन (एनजीडीओ)
- धर्मार्थ संगठन
- समर्थन संगठन
- ऐसे संगठनों के नेटवर्क या संघ
- साथ ही पेशेवर सदस्यता संघ।
नीति के अंतर्गत शामिल होने के लिए, स्वैच्छिक संगठनों में मोटे तौर पर निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए:
- वे निजी हैं, यानी सरकार से अलग
- वे अपने मालिकों या निदेशकों को अर्जित लाभ वापस नहीं करते हैं
- वे स्वशासी हैं, अर्थात, सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं हैं
- वे परिभाषित उद्देश्यों और उद्देश्यों के साथ पंजीकृत संगठन या अनौपचारिक समूह हैं।
- नीति के उद्देश्य
- नीति के विशिष्ट उद्देश्य नीचे सूचीबद्ध हैं:
स्वैच्छिक संगठनों के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना जो उनके उद्यम और प्रभावशीलता को प्रोत्साहित करता है, और उनकी स्वायत्तता की रक्षा करता है;
स्वैच्छिक संगठनों को भारत और विदेशों से वैध रूप से आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने में सक्षम बनाना;
उन प्रणालियों की पहचान करना जिनके द्वारा सरकार स्वैच्छिक संगठनों के साथ परस्पर विश्वास और सम्मान के सिद्धांतों के आधार पर और साझा जिम्मेदारी के साथ काम कर सकती है; तथा,
स्वैच्छिक संगठनों को शासन और प्रबंधन की पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए एक सक्षम वातावरण की स्थापना
स्वैच्छिक संगठनों की स्वतंत्रता उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताकतों को चुनौती देने के लिए विकास के वैकल्पिक प्रतिमानों का पता लगाने की अनुमति देती है जो सार्वजनिक हित के खिलाफ काम कर सकते हैं और गरीबी, अभाव और अन्य सामाजिक समस्याओं से निपटने के नए तरीके खोज सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि स्वैच्छिक संगठनों से संबंधित सभी कानून, नीतियां, नियम और विनियम स्पष्ट रूप से उनकी स्वायत्तता की रक्षा करते हैं, साथ ही साथ उनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित करते हैं।
स्वैच्छिक संगठनों को केंद्र या राज्य के कानूनों के तहत सोसाइटियों के रूप में, धर्मार्थ ट्रस्टों के रूप में या गैर-लाभकारी कंपनियों के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। कुछ राज्यों ने संशोधनों के साथ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860) को अपनाया है, जबकि अन्य में स्वतंत्र कानून हैं। इसी तरह, सभी राज्यों में धर्मार्थ ट्रस्टों से संबंधित कानून अलग-अलग हैं। समय के साथ, इनमें से कई कानून और उनके अनुरूप नियम जटिल और प्रतिबंधात्मक हो गए हैं, जिससे देरी, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार हुआ है। सरकार और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच इंटरफेस के लिए नोडल एजेंसी के रूप में, योजना आयोग राज्य सरकारों को प्रचलित कानूनों और नियमों की समीक्षा करने और जहां तक संभव हो उन्हें सरल, उदार और तर्कसंगत बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। गैर-लाभकारी कंपनियों के पंजीकरण की सुविधा के लिए, सरकार कंपनी अधिनियम (1956) की धारा 25 के तहत प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उपायों की जांच करेगी, जिसमें सदस्य-कर्मचारियों को लाइसेंस, पंजीकरण और पारिश्रमिक शामिल हैं।
सरकार एक सरल और उदार केंद्रीय कानून बनाने की व्यवहार्यता की भी जांच करेगी जो स्वैच्छिक संगठनों को पंजीकृत करने के लिए एक वैकल्पिक अखिल भारतीय क़ानून के रूप में काम करेगा, विशेष रूप से वे जो देश के विभिन्न हिस्सों और यहां तक कि विदेशों में भी काम करना चाहते हैं। ऐसा कानून प्रचलित केंद्रीय और राज्य कानूनों के साथ सह-अस्तित्व में होगा, जिससे वीओ को अपनी गतिविधियों की प्रकृति और क्षेत्र के आधार पर एक या एक से अधिक कानूनों के तहत पंजीकरण करने का विकल्प मिलेगा।
स्वैच्छिक क्षेत्र, विशेष रूप से इसके शासन, जवाबदेही और पारदर्शिता पर बहुत सार्वजनिक बहस हुई है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि स्वैच्छिक क्षेत्र को इन मुद्दों को उपयुक्त स्व-नियमन के माध्यम से संबोधित करना चाहिए। सरकार स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र, राष्ट्रीय स्तर, स्व-नियामक एजेंसी के विकास को प्रोत्साहित करेगी और बाद में उसे मान्यता प्रदान करेगी।
साथ ही, स्वैच्छिक क्षेत्र को अधिक से अधिक सार्वजनिक जांच के लिए खोलकर जनता के विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार केंद्र और राज्य स्तर की एजेंसियों को स्वैच्छिक संगठनों के संबंध में बुनियादी दस्तावेज दाखिल करने के लिए मानदंड पेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जो सरकारी एजेंसियों द्वारा वित्त पोषण प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें सार्वजनिक डोमेन (इंटरनेट के माध्यम से आसान पहुंच के साथ) में रखने के लिए एक भावना पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। सार्वजनिक निरीक्षण का।
स्वैच्छिक संगठनों का अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण ऐसे संगठनों और देश में उनके काम का समर्थन करने में एक छोटा, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विदेशी फंडिंग चाहने वाले संगठन को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। यह कानून कड़े स्क्रीनिंग मानदंड निर्धारित करता है जो अक्सर विदेशी निधियों का लाभ उठाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों की क्षमता को प्रतिबंधित करता है। स्वीकृत होने पर, एक ही बैंक खाते में धन रखने जैसी समस्याएं होती हैं, इस प्रकार विभिन्न स्थानों पर काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों के लिए भारी कठिनाइयाँ होती हैं। सरकार एफसीआरए की समीक्षा करेगी और संबंधित मंत्रालय द्वारा स्थापित किए जाने वाले संयुक्त सलाहकार समूह के परामर्श से समय-समय पर स्वैच्छिक संगठनों पर लागू होने वाले प्रावधानों को सरल बनाएगी।
केंद्र सरकार ने द्विपक्षीय एजेंसियों को सामाजिक और आर्थिक महत्व की परियोजनाओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों को प्रत्यक्ष सहायता देने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। यह एफसीआरए के माध्यम से और आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा विनियमन के माध्यम से इस तरह के फंड तक पहुंच और उनके उपयोग को नियंत्रित करता है। संबंधित मंत्रालय द्वारा स्थापित किए जाने वाले संयुक्त सलाहकार समूह के परामर्श से इस प्रणाली को सरल बनाने की आवश्यकता है।
सरकार सभी संबंधित केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों को स्वैच्छिक क्षेत्र के साथ रचनात्मक संबंधों पर सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। ऐसी एजेंसियों को स्वैच्छिक संगठनों से निपटने के लिए समयबद्ध प्रक्रियाएं शुरू करनी चाहिए। इनमें पंजीकरण, आयकर मंजूरी, वित्तीय सहायता आदि शामिल होंगे। शिकायतों को दर्ज करने और स्वैच्छिक संगठनों की शिकायतों के निवारण के लिए औपचारिक प्रणाली होगी।
Sanjay Kumar

 Chat with Us
Chat with Us